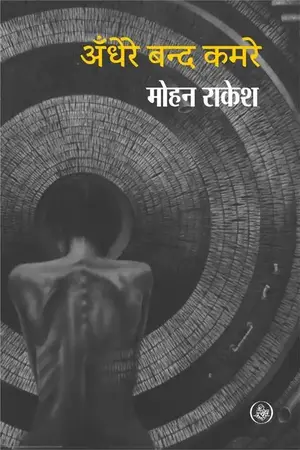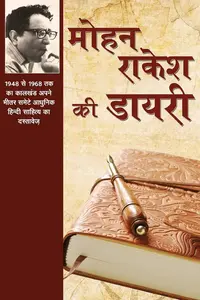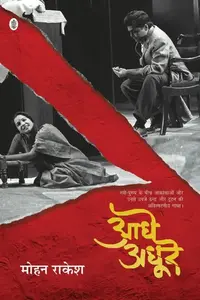|
उपन्यास >> अँधेरे बंद कमरे अँधेरे बंद कमरेमोहन राकेश
|
223 पाठक हैं |
|||||||
"परंपरा और आधुनिकता के बीच : अभिजात वर्ग में पहचान की खोज"
Andhere Band kamare a hindi book by Mohan Rakesh - अँधेरे बंद कमरे - मोहन राकेश
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वर्तमान भारतीय समाज का अभिजातवर्गीय नागर मन दो हिस्सों में विभाजित है-एक में है पश्चिमी आधुनिकतावाद और दूसरे में वंशानुगत संस्कारवाद। इससे इस वर्ग के भीतर जो द्वंद्व पैदा होता है, उससे पूर्वता के बीच रिक्तता, स्वच्छंदता के बीच अवरोध और प्रकाश के बीच अंधकार आ खड़ा होता है। परिणामतः व्यक्ति ऊबने लगता है, भीतर-ही-भीतर क्रोध, ईर्ष्या और संदेह जकड़ लेते हैं उसे, जैसे वह अपने ही लिए अजनबी हो। उठता है वह, और तब इसे हम हरबंस की शक्ल में पहचानते हैं। हरबंस, इस उपन्यास का केन्द्रीय पात्र है जो दाम्पत्य संबंधों की तलाश में भटक रहा है। हरबंस और नीलिमा के माध्यम से पारस्परिक ईमानदारी, भावनात्मक लगाव और मानसिक समदृष्टि से रिक्त दांपत्य जीवन का यहाँ प्रभावशाली चित्रण हुआ है। अपनी पहचान के लिए पहचानहीन होते जा रहे भारतीय अभिजातवर्ग की भौतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक महत्त्वाकांक्षाओं के अँधेरे बंद, कमरों को खोलनेवाले यह उपन्यास हिंदी की गिनी-चुनी कथाकृतियों में से एक है।
भूमिका में क्या होना चाहिए ? उपन्यास का परिचय ? अपने दृष्टिकोण का उल्लेख मगर दृष्टिकोण का उल्लेख भूमिका में करना हो, तो उपन्यास लिखने की क्या जरूरत है ?
और जहाँ तक परिचय का सवाल है, मैं सोचकर भी तय नहीं कर पा रहा है इसे क्या कहूँ : आज की दिल्ली का रेखाचित्र ? पत्रकार मधुसूदन की आत्मकथा ? हरबंस और नीलिमा के अन्तर्द्वन्द्व की कहानी ?
‘‘हवा में कहीं एक कोहेनूर झिलमिलाता है...’’
उस कोहेनूर का किस्सा ?
सच मैं तय नहीं कर पा रहा। पढ़कर आप जो भी निश्चय करें वही ठीक होगा। और अगर आप भी निश्चय न कर सकें, तो यह समस्या किसी और के लिए छोड़कर मेरी तरह अलग हो रहें।
और जहाँ तक परिचय का सवाल है, मैं सोचकर भी तय नहीं कर पा रहा है इसे क्या कहूँ : आज की दिल्ली का रेखाचित्र ? पत्रकार मधुसूदन की आत्मकथा ? हरबंस और नीलिमा के अन्तर्द्वन्द्व की कहानी ?
‘‘हवा में कहीं एक कोहेनूर झिलमिलाता है...’’
उस कोहेनूर का किस्सा ?
सच मैं तय नहीं कर पा रहा। पढ़कर आप जो भी निश्चय करें वही ठीक होगा। और अगर आप भी निश्चय न कर सकें, तो यह समस्या किसी और के लिए छोड़कर मेरी तरह अलग हो रहें।
1
नौ साल में चेहरे काफी बदल जाते हैं; और कोई-कोई चेहरा तो इतना बदल जाता है कि पहले के चेहरे के साथ उसकी कोई समानता ही नहीं रहती।
मैं नौ साल के बाद दिल्ली आया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे लिए यह एक बिल्कुल नया और अपरिचित शहर हो। जिन लोगों के साथ कभी मेरा रोज़ का उठना-बैठना था, उनमें से कई-एक तो अब बिल्कुल ही नहीं पहचाने थे; उनके नयन-नक्श वही थे, मगर उनके चेहरे के आसपास की हवा बिल्कुल और हो गयी थी। हम लोग कभी आमने-सामने पड़ जाते, तो हल्की-सी ‘हलो-हलो’ के बाद एक-दूसरे के पास से निकल जाते। और ‘हलो’ कहने में केवल होंठ ही हिलते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे। कई बार मुझे लगता कि शायद मेरे चेहरे की हवा भी इस बीच इतनी बदल गयी है कि परिचय का सूत्र फिर से जोड़ने में दूसरे को भी मेरी तरह ही कठिनाई का अनुभव होता है।
हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो काफ़ी खुलकर मिले और जिनसे काफ़ी खुलकर बातें हुईं, मगर उनके पास बैठकर भी मुझे महसूस होता रहा कि हम लोगों के बीच कहीं एक लकीर है-बहुत पतली-सी लकीर, जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर पाते और उसके इधर-उधर से हाथ बढ़ाकर ही आपस में मिलते हैं। कहाँ क्या बदल गया है, यह ठीक से मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके चेहरे-मोहरे में ज़रा भी फर्क नहीं आया था। मेरे बाल कनपटियों के पास से सफ़ेद होने लगे थे, मगर उनके बाल अब भी उतने ही काले थे जितने नौ साल पहले, यहाँ तक की कभी-कभी मुझे शक होता था कि वे सिर पर खिजाब तो नहीं लगाते। मगर उनके गालों की चमक भी वैसी ही थी और उनके ठहाकों की आवाज़ भी उसी तरह गूँजती थी, इसलिए मुझे मजबूरन सोचना पड़ता था कि खिजाबवाली बात भी गलत ही होनी चाहिए। फिर भी कई क्षण ऐसे आते थे जब वे परिचित चेहरे मुझे बहुत ही अपरिचित और बेगाने प्रतीत होते थे।
हरबंस को नौ साल के बाद मैंने पहली बार देखा; उसका चेहरा मुझे और चेहरों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा बदला हुआ लगा। उसके गालों का मांस कुछ थल-थला गया था जिससे वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा था। (उसे देखते ही पहला विचार मेरे दिमाग में यह आया कि क्या मैं भी अब उतना ही बड़ा लगने लगा हूँ ?) उसके सिर के बाल काफ़ी उड़ गये थे, जिससे उसे देखते ही सिलविक्रन के विज्ञापन की याद हो आती थी। मैं उस समय सिन्धिया हाउस के स्टाप पर बस से उतरा था और कॉफ़ी की एक प्याली पीने के इरादे से कॉफ़ी हाउस की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखते ही हरबंस पर नज़र पड़ी, तो मैं और भी चौंक गया। मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इस बार दिल्ली में उससे मुलाकात होगी। नौ साल पहले जब मैं यहाँ से गया था, तब से मेरे लिए वह विदेश में ही था। मैं सोचता था कि मेरे एक और दोस्त की तरह, जिसने पोलैण्ड की एक विधवा से शादी करके वहीं घर बसा लिया है, वह भी शायद बाहर ही कहीं बस-बसा गया होगा। जाने से पहले वह कहता भी यही था कि अब वह लौटकर इस देश में कभी नहीं आयेगा।
‘हरबंस, तुम ?’ मैं ठिठककर उसके लम्बे डीलडौल को देखता रह गया। वह हाथों में दो-एक पैकेट सँभाले बहुत उतावली में मेरी तरफ़ आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी जिससे मुझे उसका बदला हुआ चेहरा भी उस समय बदला हुआ नहीं लगा। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा अपनी पैकट वाली बाँह मेरे कन्धे पर रखकर मुझे अपने साथ सटा लिया।
‘अरे, तुम यहाँ कैसे, मधुसूदन ?’ उसने कहा। ‘मैंने तो समझा था कि तुम अब बिल्कुल अखबारनवीस ही हो गये हो और दिल्ली में तुम्हारा बिल्कुल आना-जाना नहीं होता। तीन साल में आज मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ।’
हम लोग जनपथ के चौराहे पर खड़े थे और मैं बत्ती का रंग बदलने की राह देख रहा था। बत्ती का रंग बदलते ही मैंने उसकी बाँह पर हाथ रखकर कहा, ‘‘आओ, पहले सड़क पार कर लें।’
मेरा यह झुकाव उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप मेरे साथ सड़क पार कर ली। सड़क पार करते ही वह रुक गया जैसे कि अपनी सीमा से बहुत आगे चला आया हो।
‘मैं एक तरह से नौ साल के बाद यहाँ आया हूँ,’ मैंने कहा। ‘बीच में मैं दो-चार बार एक-एक दिन के लिए आया था, मगर वह आना तो न आने के बराबर ही था।’
मगर मुझे लगा कि उसने मेरी बात की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। उसकी आँखें मेरे कन्धों के ऊपर से सड़क के पार किसी चीज़ को खोज रही थीं।
‘तुम बाहर से कब आये हो ?’ मैंन पूछा। ‘मैंने तो सोचा था कि तुम अब बाकी ज़िन्दगी लन्दन या पेरिस में ही कहीं काट दोगे। जाने से पहले तुम्हारा इरादा भी यही था।’ यह कहते हुए मुझे सहसा नीलिमा के नाम लिखे उसके पत्रों की याद हो आयी, और मेरा मन एक विचित्र उत्सुकता से भर गया।
‘मुझे आये तीन साल हो गये,’ वह उसी तरह मोटरों और बसों की भीड़ में कुछ खोजता हुआ बोला, ‘बल्कि अब यह चौथा साल जा रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम लखनऊ के किसी दैनिक में हो। दैनिक का नाम भी उसने बताया था। मैंने एकाध बार सोचा भी कि तुम्हें चिट्ठी लिखूँ, मगर ऐसे ही आलस में बात रह गयी। तुम जानते हो चिट्ठियाँ लिखने के मामले में मैं कितना आलसी हूँ।’
मुझे फिर उन दिनों की याद हो आयी जब वह अभी बाहर गया ही था। उन दिनों भी क्या वह चिट्ठियाँ लिखने के बारे में ऐसी बात कह सकता था ? मेरे होंठों पर मुस्कराहट की एक हल्की-सी लकीर आ गयी और मैंने कहा, ‘हो सकता है, मगर इसमें सिर्फ नीलिमा की बात तुम्हें छोड़ देनी चाहिए।’
वह इससे थोड़ा सकपका गया। सहसा उसके हाथ इस तरह हिले जैसे अपनी खोयी हुई चीज़ उसे भीड़ में नज़र आ गयी हो, मगर दूसरे ही क्षण उसके कन्धे ढीले हो गये और उसके चेहरे पर निराशा की लहरें खिंच गयीं।
‘तुम किसी को ढूँढ रहे हो ?’ मैंने पूछा।
‘नहीं, देख रहा हूँ कि कोई स्कूटर मिल जाये, तो तुम्हें अपने घर ले चलूँ।’
उसका यह सोच लेना कि मुझे साथ घर ले जाने के लिए उसका मुझसे पूछना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरन्त ही मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा।
‘आज हमारे यहाँ कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसलिए मेरा जल्दी घर पहुँचना जरूरी है,’ वह बोला। ‘नीलिमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। अभी आठ ही दस दिन हुए जब हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं उससे कह रहा था कि जीवन भार्गव की तरह यह आदमी भी ज़िन्दगी के दलदल में फँसकर रह गया। घर चलो, तो वहाँ तुम्हें एक नया व्यक्ति भी मिलेगा जिससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी।’
‘नया व्यक्ति ?’
‘हमारा लड़का अरुण। वह अब तीन साल का होने जा रहा है। एक बार तुम्हें पहचान लेगा, तो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आओ, उधर स्कूटर स्टैण्ड पर चलते हैं। यहाँ पर खड़े-खड़े कोई स्कूटर नहीं मिलेगा।’
‘मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकूँगा,’ मैंने कहा। ‘फिर किसी दिन चलूँगा। या तुम मुझे घर का पता बता दो, मैं अपने-आप किसी दिन पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे कोई तकल्लुफ तो है नहीं।’ और यह कहते हुए मुझे उलझन हुई कि मेरी यह बात भी तकल्लुफ नहीं, तो और क्या है ?
‘फिर किसी दिन खाक आओगे।’ वह थोड़ा खीझ गया। ‘कल-परसों जाकर लखनऊ से चिट्ठी लिख दोगे कि मुझे अफ़सोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। और हो सकता है कि चिट्ठी भी न लिखो।’
‘नहीं, अब इस तरह का मौका नहीं आ सकता,’ मैंने कहा। ‘मैं लखनऊ छोड़कर दिल्ली में आ गया हूँ।’
‘क्या !’ आश्चर्य से उसके हाथ का पैकेट गिरने को हो गया जिसे उसने किसी तरह सँभाल लिया। तुम लखनऊ से नौकरी छोड़ आये हो ?’
‘हाँ।’
‘कब से ?’
‘वहाँ से रिलीव हुए मुझे दस दिन हो गये। पिछले मंगल से मैंने यहाँ ‘न्यू हैरल्ड’ में जॉइन कर लिया है। अब दूसरा मंगल है।’
‘सच ?’
‘हाँ, सच नहीं तो क्या ?’
‘यह सुनकर नीलिमा तो बहुत ही खुश होगी’, उसने दोनों पैकेट एक साथ में लेकर दूसरे हाथ से मेरी बाँह को पकड़ लिया। ‘इस वक्त तो तुम्हें हर हालत में मेरे साथ चलना ही है। नीलिमा को पता चलेगा कि तुम दिल्ली में हो और फिर भी मेरे साथ घर नहीं आये, तो वह कितना बुरा मानेगी ? आओ, चलो...।’
‘नहीं, इस वक्त मैं सचमुच नहीं चल सकूँगा’, मैंने अपनी बाँह उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। ‘अभी मैं बस से उतरा ही हूँ और पहले कॉफ़ी की एक प्याली पीना चाहता हूँ। और कॉफ़ी हाउस में मैंने किसी से मिलने के लिए भी कह रखा है।’
‘ऐसा कौन आदमी है जिससे मिलना इतना ज़रूरी है ?’
‘है एक आदमी,’ मैंने कहा। ‘तुम उसे नहीं जानते।’ मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मैंने फट से किसी का भी नाम क्यों नहीं ले दिया। झूठ बोलते वक्त जाने ज़बान कुछ जकड़ क्यों जाती है ? इससे झूठ बोलने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता और दूसरे को भी फ़ौरन पता चल जाता है कि बात झूठ कही गयी है।
‘तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ’, वह बोला। ‘कॉफ़ी की एक प्याली पी लो और उस आदमी को जिस-किसी तरह टाल दो। घर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा।’
मैं अपना हठ चुका था और किसी से मिलने की बात थी नहीं, इसलिए मेरा मन हुआ कि अब मैं सीधा उसके साथ चला जाऊँ। मगर अपनी बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैंने कहा, ‘अच्छा आओ, वहाँ चलकर देख लेते हैं। उससे छः बजे मिलने की बात थी। वह नहीं, मिला, तो मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा। अपनी तरफ़ से तो मैं उसके सामने सच्चा रहूँगा कि वक्त पर पहुँच गया था।’
जनपथ के कॉरिडॉर में उसके साथ चलते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे कि वे नौ साल पहले के ही दिन हों जब हम कितनी ही बार इस तरह साथ-साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाया करते थे, हालाँकि उसके साथ तब मेरा परिचय बहुत थोड़े दिनों का था और जब परिचय हुआ था, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक बार के बाद ज़िन्दगी में कभी दूसरी बार भी मेरी उससे मुलाकात होगी।
मैं उन दिनों बम्बई में था और ‘काला घोड़ा’ के पास एक थर्ड क्लास होटल में दूसरी मंज़िल की एक डार्मिटरी में रहता था। मुझे बम्बई में रहते दो साल हो चुके थे और मैं वहाँ की ज़िन्दगी से बुरी तरह ऊबा हुआ था। बम्बई जैसे शहर में आदमी के पास जीने की सुविधाएँ न हों, तो उसके पास ऊबकर वहाँ से चले आने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। मैं दो साल में वहां प्रूफरीडरी से लेकर फुटपाथ पर सोने तक सभी तरह के अनुभव प्राप्त कर चुका था और अब वहाँ से लौटने की तैयारी में था। एक रात जब मैं होटल की मालकिन के दिये हुए खाने पर कुढ़ रहा था, तो मेरा मित्र प्रेम लूथरा अचानक अपने एक और मित्र के साथ मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ। उसने सरसरी तौर पर अपने मित्र का परिचय दिया, ‘‘हरबंस खुल्लर। हम लोग एम.ए. में साथ-साथ पढ़ते थे। मैंने इसे तुम्हारी कुछ-एक कविताएँ सुनायी थीं। इस वक्त घूमने के लिए निकले, तो मैंने कहा, चलो तुम्हें उन कविताओं के लेखक से भी मिला दूँ।’
ठण्डे गोश्त के स्लाइस मुझसे खाये नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने छुरी-काँटा प्लेट में पटककर उसे अलग हटा दिया। बैरा आकर प्लेट उठाने लगा, तो मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि उन्हें ठण्डा गोश्त खाने का शौक हो, तो उनके लिए मँगवा दूँ।’
‘हम लोग खा चुके हैं’, प्रेम ने कहा, ‘मगर तुम लगता है, भूखे रह गये हो। चलो, तुम्हें चलकर किसी रेस्तराँ में कुछ ख़िला दें। भूखे पेट तुम ठीक से बात नहीं कर सकोगे। इसे तुम्हारी कविताएँ बिल्कुल पसन्द नहीं आयीं, इसलिए अच्छा है पहले तुम कु़छ खा-पीकर अपने को स्वस्थ कर लो।’ और वह एक बेलाग हँसी हँसा। मेरा मन उसकी हँसी से हमेशा चिढ़ जाता था। वह ऐसे हँसता था जैसे दूसरे आदमी से किसी पुरानी अदावत का बदला ले रहा हो।
हम लोग वहाँ से उठकर नीचे एक निरामिष भोजनालय में आ गये और घण्टा-डेढ़ घण्टा वहाँ बैठकर बातें करते रहे। उस बातचीत में मुझे पता चला कि हरबंस दिल्ली के किसी कॉलेज में इतिहास पढ़ाता है। मगर वह बातें इस तरह कर रहा था जैसे उसका वास्तविक विषय इतिहास न होकर इतिहास के अलावा और सभी कुछ हो। वह साहित्य से लेकर राजनीति तक और नृत्य से लेकर विदेशी मिशनरियों तक-न जाने कितने विषयों पर बहुत ही अधिकारपूर्ण ढंग से कितना कुछ कहता रहा। चेख़व, दॉस्तॉएव्स्की, लियोनार्दो दा विंसी, पिकासो, उदयशंकर, पण्डित नेहरू और बिशप ऑफ़ लाहौर-इन सबके बारे में वह इस तरह बात कर रहा था जैसे इन सबसे उसका निजी परिचय हो, और वह मेरे ऊपर इस बात का रौब जमाना चाहता हो कि वह स्वयं भी उस बिरादरी का ही आदमी है। उसके लिए रहस्यवाद, क्यूबिज़्म और कथाकलि, ये सब जैसे घर के ही शब्द थे, जिनका वह बहुत सरसरी तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। मुझे कोफ़्त हो रही थी कि वह ख़ामख़ाह मेरे ऊपर रौब क्यों झाड़ रहा है। मगर मैं किसी तरह धीरज के साथ उसकी बातें सुनता रहा। सोचा कि कहीं वह यह न समझे कि मैं इसलिए उसकी बातों से चिढ़ रहा हूँ कि उसे मेरी कविताएँ पसन्द नहीं आयीं। बल्कि मेरी कविताओं के बारे में उसने जो कुछ कहा था उससे मुझे लगा था जैसे वह मेरी बात न करके किसी अच्छे-ख़ासे प्रतिष्ठित कवि की बात कर रहा हो और उसकी त्रुटियाँ बताकर उसे मेरे ऊपर अपनी सूझ-बूझ का सिक्का ही बैठाना हो ! मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी कविताओं के बारे में भी इस तरह गम्भीरतापूर्वक बात कर सकता है। हम लोग जब भोजनालय से बाहर निकले, तो मैं बहुत कठिनाई से अपनी जम्हाइयों को रोके हुए था और चाह रहा था कि किसी तरह बातचीत का सिलसिला समाप्त हो, तो जाकर सो जाऊँ। रोज़ सुबह चार बजे ही ट्रामों की घरड़-घरड़ और टनन-टनन की वजह से नींद टूट जाती थी जिससे दिन-भर दिमाग़ की नसें तनी रहती थीं। आख़िर फ्लोरा फ़ाउण्टेन तक जाकर मैंने उन लोगों से विदा ली। चलते समय कहा कि मैं दिल्ली आऊँ, तो उससे ज़रूर मिलूँ। मैंने जल्दी ही इसकी हामी भर दी कि कहीं बात और लम्बी न हो जाये। उन्हें छोड़कर लौटते हुए मैं कुछ देर ‘एयर एण्डिया’ के दफ़्तर के बाहर मूँछ और पगड़ीवाले बौने की सूक्तियाँ पढ़ता रहा कि किसी तरह मन की ऊब और झुँझलाहट कुछ कम हो, तो जाकर सोने की कोशिश करूँ। मगर जहाँ तक मुझे याद है, उस रात मुझे तब तक नींद नहीं आयी जब तक नीचे ट्रामों ने सुबह की घण्टियाँ बजाना आरम्भ नहीं कर दिया।
थोड़े दिनों बाद मैं बम्बई छोड़कर दिल्ली चला गया। हरबंस और उसके सारे साहित्य और कला सम्बन्धी बात मैं बम्बई में ही भूल आया था। दिल्ली आकर मैं अपने मित्र अरविन्द के पास ठहरा था जो उन दिनों एक हिन्दी दैनिक में सहायक सम्पादक के रूप में काम कर रहा था। अरविन्द क़स्साबपुरा में अपने प्रेस के एक दफ़्तरी के साथ रहता था। दफ़्तरी, जिसे वहाँ सब लोग ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे, क़स्साबपुरा के उस मुसलमान मुहल्ले में एक टूटे-फूटे घर में नीचे की दो कोठरियों पर कब्जा किये हुए था जिनमें से आगे की कोठरी में अरविन्द रहता था और पीछे की कोठरी में वह स्वयं अपनी पत्नी और सात-आठ साल की लड़की के साथ रहता था। अरविन्द खाना भी उसके यहाँ से ही खाता था और उसे कुल मिलाकर पचहत्तर रुपये महीने देता था। मेरे आने पर पच्चीस, रुपये महीने और देकर उसने मेरे खाने की व्यवस्था भी साथ ही कर दी। दफ़्तरी की पत्नी, जिसे हम कभी ठकुराइन और कभी भाभी कहकर बुलाते थे, बहुत स्नेह और चाव में हमें खिलाती थी। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि वह ठाकुर साहब को उतना अच्छा खाना नहीं देती जितना अच्छा हमें देती है। अरविन्द की जब दिन की ड्यूटी होती थी, तो वह दोपहर का खाना साथ दफ़्तर ले जाता था और जब रात की ड्यूटी होती थी तो ठकुराइन बारह-एक बजे आने पर भी उसे खाना गरम करके ही खिलाती थी। खाना खाते समय अरविन्द ठकुराइन से कुछ-न-कुछ चुहल करता रहता था। ‘ठकुराइन, तर माल तो तुम सब ठाकुर साहब को देती हो; हमारे आगे तो जो रुखा-सूखा बच जाता है वही रख देती हो।’ वह कहता।
‘अभी तुम तर माल के लायक हो कहाँ, लाला ?’ ठकुराइन हँसकर कहती। ‘अभी तो तुम बच्चे हो। तर माल खाओगे, तो बिगड़ नहीं जाओगे ?’’
‘तुम तो ठकुराइन सारी उम्र हमें बच्चा ही बनाये रखोगी,’ अरविन्द कहता। ‘आख़िर हमें किसी तरह बड़े भी तो होना है। हमें कभी तो कुछ खिलाया करो।’
जब खाने लायक हो जाओगे, तो माँगकर नहीं खाओगे,’ ठकुराइन हँसती रहती, ‘पतीली में से निकाल कर खा जाया करोगे। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी, उस दिन ठकुराइन को नहीं पूछोगे। जहाँ पतीली देखोगे, वहीं मुँह मारने लगोगे।’ कहते-कहते ठकुराइन को न जाने क्या लगता कि वह सिर कपड़ा ठीक कर लेती। अपनी मैली धोती के सूराख भी वह जिस किसी तरह ढक लेती।
‘इस तरह कहीं मुँह मारेंगे, तो जूती नहीं खायेंगे ?’ अरविन्द कहता।
‘पकड़े जाओगे तो जूती भी खाओगे। मगर जो जूती से डरता हो, उसे तर माल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, छोटे लाला ?’
मैं हूँ-हाँ में उत्तर देकर कम्बल ओढ़ लेता। ठकुराइन फिर कहती, ‘हमारे छोटे लाला तो बिल्कुल साधु-सन्त आदमी हैं। इन्हें तो रूखा-सूखा भी न मिले, तो भी इनका पेट भरा रहता है। मेरा तो खयाल है इन्हें भूख लगती ही नहीं।’
अरविन्द मेरे चिकुटी काट देता। ‘क्यों बे, बोलता क्यों नहीं ?’
‘ठकुराइन ठीक कहती हैं,’ मैं कम्बल उतारकर कहता।
‘क्या ठीक कहती हैं ?’
‘कि मुझे भूख नहीं लगती। आज सुबह गोभी की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, फिर भी मुझसे सिर्फ़ दो ही रोटी खायी गयीं।’
‘धत्तेरे की !’ अरविन्द मेरे बालों में उँगलियाँ उलझाकर मेरे सिर को अच्छी तरह मल देता ।‘तुझे गोभी के सिवा कुछ सूझता भी है ?’
मैं चुप रहता, क्योंकि मुझे उस समय यह सूझ रहा होता कि कहीं साथ की कोठरी में ठाकुर साहब के खर्राटे सहसा बन्द न हो जायें और मुँह से कुछ कहते-न-कहते मुँह का जायका ही न बदल जाये।
ठकुराइन सिर पर कपड़ा फिर ठीक करती और आँखों-ही-आँखों में मुस्कुराती हुई कहती, ‘ये देखे में जितने सीधे लगते हैं, असल में उतने सीधे हैं नहीं। दुनिया-भर के सब माल खाये हुए हैं। बम्बई रहकर आये हैं। वहाँ तो सुना है कि भाँत-भाँत के पदारथ मिलते हैं।’
अरविन्द एक हाथ से कौर मुँह में डालता और दूसरे हाथ से फिर मुझे थोड़ा गुदगुदा देता और कहता, ‘ठकुराइन, हमारी न सही, कभी तुम इसकी ही कुछ खातिर करो। यह भी क्या कहेगा कि हाँ बम्बई के बाद दिल्ली में भी कुछ दिन रहे थे...’
‘इनसे कहो, ये कहें अपने मुँह से ! बस एक बार कह दें, तो देखो ठकुराइन इनकी ख़ातिरदारी के लिए क्या-क्या नहीं करती ? रोज़ कहें तो रोज़ उन्हें घी की पूरी बनाकर खिलाऊँ।’
‘क्यों बे !’’ अरविन्द अपने जूठे गिलास में हाथ धोकर मुँह पर फेरता हुआ कहता। ‘एक बार कह क्यों नहीं देता ? तेरे बहाने हमें भी घी की पूरी मिल जायेगी। भाभी को तुम ऐसी-वैसी मत समझना, इसका दिल-गुर्दा बहुत बड़ा है।’
‘किससे कह रहे हो लाला ?’ ठकुराइन उसके जूठे बरतन उठाकर चल देती। ‘बेचारे सन्त-महात्मा के पेट में क्यों चूहे दौड़ाते हो ? अभी तो इन्हें तुम नौकरी की ही बात सोचने दो। नौकरी हो जायेगी, तो दुनिया-भर के तर माल भी अपने-आप उड़ाने को मिल जायेंगे। अभी इन्हें तुम रूखे-सूखे पर ही रहने दो।’
ठकुराइन जाकर अपनी कोठरी का किवाड़ बन्द कर लेती, तो अरविन्द कम्बल ओढ़कर लम्बा होता हुआ धीरे से कहता, ‘ठकुराइन है रंगीन-मिज़ाज ! है कि नहीं ?’
‘हाँ है,’ मैं कुढ़े हुए स्वर में कहता। ‘अब मुझे सोने दो।’
‘अच्छा बताओ, तुम क्या सोच रहे हो ? अरविन्द करवट बदलकर मेरे ऊपर को झुका आता।
‘नौकरी की बात सोच रहा हूँ।’
‘धत्त !’ वह मेरी जाँघ को हाथ से मसल देता।‘जैसे नौकरी की बात सोचने का यही वक्त है।’
‘तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकार आदमी हर वक्त एक ही बात सोचता है।’
‘अच्छा यार एक बता बताओ।’ उसका स्वर बहुत धीमा और रहस्यपूर्ण हो जाता।
‘अगर ठकुराइन को थोड़ा और टटोला जाये, तो तुम्हारा क्या ख़याल है इसे पटाया जा सकता है ?’
मैं उसे गुस्से में परे धकेल देता। ‘अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।’
‘मैं तो समझता हूँ कि बस दाना डालने की बात है’, वह सीधा पड़ा-पड़ा कहता। ‘अगर ठीक से दाना डाला जाये तो ऐसी कोई बात नहीं कि ठकुराइन मान न जाये।’
मैं नौ साल के बाद दिल्ली आया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे लिए यह एक बिल्कुल नया और अपरिचित शहर हो। जिन लोगों के साथ कभी मेरा रोज़ का उठना-बैठना था, उनमें से कई-एक तो अब बिल्कुल ही नहीं पहचाने थे; उनके नयन-नक्श वही थे, मगर उनके चेहरे के आसपास की हवा बिल्कुल और हो गयी थी। हम लोग कभी आमने-सामने पड़ जाते, तो हल्की-सी ‘हलो-हलो’ के बाद एक-दूसरे के पास से निकल जाते। और ‘हलो’ कहने में केवल होंठ ही हिलते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे। कई बार मुझे लगता कि शायद मेरे चेहरे की हवा भी इस बीच इतनी बदल गयी है कि परिचय का सूत्र फिर से जोड़ने में दूसरे को भी मेरी तरह ही कठिनाई का अनुभव होता है।
हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो काफ़ी खुलकर मिले और जिनसे काफ़ी खुलकर बातें हुईं, मगर उनके पास बैठकर भी मुझे महसूस होता रहा कि हम लोगों के बीच कहीं एक लकीर है-बहुत पतली-सी लकीर, जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर पाते और उसके इधर-उधर से हाथ बढ़ाकर ही आपस में मिलते हैं। कहाँ क्या बदल गया है, यह ठीक से मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके चेहरे-मोहरे में ज़रा भी फर्क नहीं आया था। मेरे बाल कनपटियों के पास से सफ़ेद होने लगे थे, मगर उनके बाल अब भी उतने ही काले थे जितने नौ साल पहले, यहाँ तक की कभी-कभी मुझे शक होता था कि वे सिर पर खिजाब तो नहीं लगाते। मगर उनके गालों की चमक भी वैसी ही थी और उनके ठहाकों की आवाज़ भी उसी तरह गूँजती थी, इसलिए मुझे मजबूरन सोचना पड़ता था कि खिजाबवाली बात भी गलत ही होनी चाहिए। फिर भी कई क्षण ऐसे आते थे जब वे परिचित चेहरे मुझे बहुत ही अपरिचित और बेगाने प्रतीत होते थे।
हरबंस को नौ साल के बाद मैंने पहली बार देखा; उसका चेहरा मुझे और चेहरों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा बदला हुआ लगा। उसके गालों का मांस कुछ थल-थला गया था जिससे वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा था। (उसे देखते ही पहला विचार मेरे दिमाग में यह आया कि क्या मैं भी अब उतना ही बड़ा लगने लगा हूँ ?) उसके सिर के बाल काफ़ी उड़ गये थे, जिससे उसे देखते ही सिलविक्रन के विज्ञापन की याद हो आती थी। मैं उस समय सिन्धिया हाउस के स्टाप पर बस से उतरा था और कॉफ़ी की एक प्याली पीने के इरादे से कॉफ़ी हाउस की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखते ही हरबंस पर नज़र पड़ी, तो मैं और भी चौंक गया। मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इस बार दिल्ली में उससे मुलाकात होगी। नौ साल पहले जब मैं यहाँ से गया था, तब से मेरे लिए वह विदेश में ही था। मैं सोचता था कि मेरे एक और दोस्त की तरह, जिसने पोलैण्ड की एक विधवा से शादी करके वहीं घर बसा लिया है, वह भी शायद बाहर ही कहीं बस-बसा गया होगा। जाने से पहले वह कहता भी यही था कि अब वह लौटकर इस देश में कभी नहीं आयेगा।
‘हरबंस, तुम ?’ मैं ठिठककर उसके लम्बे डीलडौल को देखता रह गया। वह हाथों में दो-एक पैकेट सँभाले बहुत उतावली में मेरी तरफ़ आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी जिससे मुझे उसका बदला हुआ चेहरा भी उस समय बदला हुआ नहीं लगा। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा अपनी पैकट वाली बाँह मेरे कन्धे पर रखकर मुझे अपने साथ सटा लिया।
‘अरे, तुम यहाँ कैसे, मधुसूदन ?’ उसने कहा। ‘मैंने तो समझा था कि तुम अब बिल्कुल अखबारनवीस ही हो गये हो और दिल्ली में तुम्हारा बिल्कुल आना-जाना नहीं होता। तीन साल में आज मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ।’
हम लोग जनपथ के चौराहे पर खड़े थे और मैं बत्ती का रंग बदलने की राह देख रहा था। बत्ती का रंग बदलते ही मैंने उसकी बाँह पर हाथ रखकर कहा, ‘‘आओ, पहले सड़क पार कर लें।’
मेरा यह झुकाव उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप मेरे साथ सड़क पार कर ली। सड़क पार करते ही वह रुक गया जैसे कि अपनी सीमा से बहुत आगे चला आया हो।
‘मैं एक तरह से नौ साल के बाद यहाँ आया हूँ,’ मैंने कहा। ‘बीच में मैं दो-चार बार एक-एक दिन के लिए आया था, मगर वह आना तो न आने के बराबर ही था।’
मगर मुझे लगा कि उसने मेरी बात की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। उसकी आँखें मेरे कन्धों के ऊपर से सड़क के पार किसी चीज़ को खोज रही थीं।
‘तुम बाहर से कब आये हो ?’ मैंन पूछा। ‘मैंने तो सोचा था कि तुम अब बाकी ज़िन्दगी लन्दन या पेरिस में ही कहीं काट दोगे। जाने से पहले तुम्हारा इरादा भी यही था।’ यह कहते हुए मुझे सहसा नीलिमा के नाम लिखे उसके पत्रों की याद हो आयी, और मेरा मन एक विचित्र उत्सुकता से भर गया।
‘मुझे आये तीन साल हो गये,’ वह उसी तरह मोटरों और बसों की भीड़ में कुछ खोजता हुआ बोला, ‘बल्कि अब यह चौथा साल जा रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम लखनऊ के किसी दैनिक में हो। दैनिक का नाम भी उसने बताया था। मैंने एकाध बार सोचा भी कि तुम्हें चिट्ठी लिखूँ, मगर ऐसे ही आलस में बात रह गयी। तुम जानते हो चिट्ठियाँ लिखने के मामले में मैं कितना आलसी हूँ।’
मुझे फिर उन दिनों की याद हो आयी जब वह अभी बाहर गया ही था। उन दिनों भी क्या वह चिट्ठियाँ लिखने के बारे में ऐसी बात कह सकता था ? मेरे होंठों पर मुस्कराहट की एक हल्की-सी लकीर आ गयी और मैंने कहा, ‘हो सकता है, मगर इसमें सिर्फ नीलिमा की बात तुम्हें छोड़ देनी चाहिए।’
वह इससे थोड़ा सकपका गया। सहसा उसके हाथ इस तरह हिले जैसे अपनी खोयी हुई चीज़ उसे भीड़ में नज़र आ गयी हो, मगर दूसरे ही क्षण उसके कन्धे ढीले हो गये और उसके चेहरे पर निराशा की लहरें खिंच गयीं।
‘तुम किसी को ढूँढ रहे हो ?’ मैंने पूछा।
‘नहीं, देख रहा हूँ कि कोई स्कूटर मिल जाये, तो तुम्हें अपने घर ले चलूँ।’
उसका यह सोच लेना कि मुझे साथ घर ले जाने के लिए उसका मुझसे पूछना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरन्त ही मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा।
‘आज हमारे यहाँ कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसलिए मेरा जल्दी घर पहुँचना जरूरी है,’ वह बोला। ‘नीलिमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। अभी आठ ही दस दिन हुए जब हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। मैं उससे कह रहा था कि जीवन भार्गव की तरह यह आदमी भी ज़िन्दगी के दलदल में फँसकर रह गया। घर चलो, तो वहाँ तुम्हें एक नया व्यक्ति भी मिलेगा जिससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी।’
‘नया व्यक्ति ?’
‘हमारा लड़का अरुण। वह अब तीन साल का होने जा रहा है। एक बार तुम्हें पहचान लेगा, तो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आओ, उधर स्कूटर स्टैण्ड पर चलते हैं। यहाँ पर खड़े-खड़े कोई स्कूटर नहीं मिलेगा।’
‘मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकूँगा,’ मैंने कहा। ‘फिर किसी दिन चलूँगा। या तुम मुझे घर का पता बता दो, मैं अपने-आप किसी दिन पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे कोई तकल्लुफ तो है नहीं।’ और यह कहते हुए मुझे उलझन हुई कि मेरी यह बात भी तकल्लुफ नहीं, तो और क्या है ?
‘फिर किसी दिन खाक आओगे।’ वह थोड़ा खीझ गया। ‘कल-परसों जाकर लखनऊ से चिट्ठी लिख दोगे कि मुझे अफ़सोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। और हो सकता है कि चिट्ठी भी न लिखो।’
‘नहीं, अब इस तरह का मौका नहीं आ सकता,’ मैंने कहा। ‘मैं लखनऊ छोड़कर दिल्ली में आ गया हूँ।’
‘क्या !’ आश्चर्य से उसके हाथ का पैकेट गिरने को हो गया जिसे उसने किसी तरह सँभाल लिया। तुम लखनऊ से नौकरी छोड़ आये हो ?’
‘हाँ।’
‘कब से ?’
‘वहाँ से रिलीव हुए मुझे दस दिन हो गये। पिछले मंगल से मैंने यहाँ ‘न्यू हैरल्ड’ में जॉइन कर लिया है। अब दूसरा मंगल है।’
‘सच ?’
‘हाँ, सच नहीं तो क्या ?’
‘यह सुनकर नीलिमा तो बहुत ही खुश होगी’, उसने दोनों पैकेट एक साथ में लेकर दूसरे हाथ से मेरी बाँह को पकड़ लिया। ‘इस वक्त तो तुम्हें हर हालत में मेरे साथ चलना ही है। नीलिमा को पता चलेगा कि तुम दिल्ली में हो और फिर भी मेरे साथ घर नहीं आये, तो वह कितना बुरा मानेगी ? आओ, चलो...।’
‘नहीं, इस वक्त मैं सचमुच नहीं चल सकूँगा’, मैंने अपनी बाँह उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। ‘अभी मैं बस से उतरा ही हूँ और पहले कॉफ़ी की एक प्याली पीना चाहता हूँ। और कॉफ़ी हाउस में मैंने किसी से मिलने के लिए भी कह रखा है।’
‘ऐसा कौन आदमी है जिससे मिलना इतना ज़रूरी है ?’
‘है एक आदमी,’ मैंने कहा। ‘तुम उसे नहीं जानते।’ मुझे अपने पर गुस्सा आया कि मैंने फट से किसी का भी नाम क्यों नहीं ले दिया। झूठ बोलते वक्त जाने ज़बान कुछ जकड़ क्यों जाती है ? इससे झूठ बोलने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता और दूसरे को भी फ़ौरन पता चल जाता है कि बात झूठ कही गयी है।
‘तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ’, वह बोला। ‘कॉफ़ी की एक प्याली पी लो और उस आदमी को जिस-किसी तरह टाल दो। घर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा।’
मैं अपना हठ चुका था और किसी से मिलने की बात थी नहीं, इसलिए मेरा मन हुआ कि अब मैं सीधा उसके साथ चला जाऊँ। मगर अपनी बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैंने कहा, ‘अच्छा आओ, वहाँ चलकर देख लेते हैं। उससे छः बजे मिलने की बात थी। वह नहीं, मिला, तो मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा। अपनी तरफ़ से तो मैं उसके सामने सच्चा रहूँगा कि वक्त पर पहुँच गया था।’
जनपथ के कॉरिडॉर में उसके साथ चलते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे कि वे नौ साल पहले के ही दिन हों जब हम कितनी ही बार इस तरह साथ-साथ कॉफ़ी पीने के लिए जाया करते थे, हालाँकि उसके साथ तब मेरा परिचय बहुत थोड़े दिनों का था और जब परिचय हुआ था, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक बार के बाद ज़िन्दगी में कभी दूसरी बार भी मेरी उससे मुलाकात होगी।
मैं उन दिनों बम्बई में था और ‘काला घोड़ा’ के पास एक थर्ड क्लास होटल में दूसरी मंज़िल की एक डार्मिटरी में रहता था। मुझे बम्बई में रहते दो साल हो चुके थे और मैं वहाँ की ज़िन्दगी से बुरी तरह ऊबा हुआ था। बम्बई जैसे शहर में आदमी के पास जीने की सुविधाएँ न हों, तो उसके पास ऊबकर वहाँ से चले आने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। मैं दो साल में वहां प्रूफरीडरी से लेकर फुटपाथ पर सोने तक सभी तरह के अनुभव प्राप्त कर चुका था और अब वहाँ से लौटने की तैयारी में था। एक रात जब मैं होटल की मालकिन के दिये हुए खाने पर कुढ़ रहा था, तो मेरा मित्र प्रेम लूथरा अचानक अपने एक और मित्र के साथ मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ। उसने सरसरी तौर पर अपने मित्र का परिचय दिया, ‘‘हरबंस खुल्लर। हम लोग एम.ए. में साथ-साथ पढ़ते थे। मैंने इसे तुम्हारी कुछ-एक कविताएँ सुनायी थीं। इस वक्त घूमने के लिए निकले, तो मैंने कहा, चलो तुम्हें उन कविताओं के लेखक से भी मिला दूँ।’
ठण्डे गोश्त के स्लाइस मुझसे खाये नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने छुरी-काँटा प्लेट में पटककर उसे अलग हटा दिया। बैरा आकर प्लेट उठाने लगा, तो मैंने उन लोगों से पूछ लिया कि उन्हें ठण्डा गोश्त खाने का शौक हो, तो उनके लिए मँगवा दूँ।’
‘हम लोग खा चुके हैं’, प्रेम ने कहा, ‘मगर तुम लगता है, भूखे रह गये हो। चलो, तुम्हें चलकर किसी रेस्तराँ में कुछ ख़िला दें। भूखे पेट तुम ठीक से बात नहीं कर सकोगे। इसे तुम्हारी कविताएँ बिल्कुल पसन्द नहीं आयीं, इसलिए अच्छा है पहले तुम कु़छ खा-पीकर अपने को स्वस्थ कर लो।’ और वह एक बेलाग हँसी हँसा। मेरा मन उसकी हँसी से हमेशा चिढ़ जाता था। वह ऐसे हँसता था जैसे दूसरे आदमी से किसी पुरानी अदावत का बदला ले रहा हो।
हम लोग वहाँ से उठकर नीचे एक निरामिष भोजनालय में आ गये और घण्टा-डेढ़ घण्टा वहाँ बैठकर बातें करते रहे। उस बातचीत में मुझे पता चला कि हरबंस दिल्ली के किसी कॉलेज में इतिहास पढ़ाता है। मगर वह बातें इस तरह कर रहा था जैसे उसका वास्तविक विषय इतिहास न होकर इतिहास के अलावा और सभी कुछ हो। वह साहित्य से लेकर राजनीति तक और नृत्य से लेकर विदेशी मिशनरियों तक-न जाने कितने विषयों पर बहुत ही अधिकारपूर्ण ढंग से कितना कुछ कहता रहा। चेख़व, दॉस्तॉएव्स्की, लियोनार्दो दा विंसी, पिकासो, उदयशंकर, पण्डित नेहरू और बिशप ऑफ़ लाहौर-इन सबके बारे में वह इस तरह बात कर रहा था जैसे इन सबसे उसका निजी परिचय हो, और वह मेरे ऊपर इस बात का रौब जमाना चाहता हो कि वह स्वयं भी उस बिरादरी का ही आदमी है। उसके लिए रहस्यवाद, क्यूबिज़्म और कथाकलि, ये सब जैसे घर के ही शब्द थे, जिनका वह बहुत सरसरी तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। मुझे कोफ़्त हो रही थी कि वह ख़ामख़ाह मेरे ऊपर रौब क्यों झाड़ रहा है। मगर मैं किसी तरह धीरज के साथ उसकी बातें सुनता रहा। सोचा कि कहीं वह यह न समझे कि मैं इसलिए उसकी बातों से चिढ़ रहा हूँ कि उसे मेरी कविताएँ पसन्द नहीं आयीं। बल्कि मेरी कविताओं के बारे में उसने जो कुछ कहा था उससे मुझे लगा था जैसे वह मेरी बात न करके किसी अच्छे-ख़ासे प्रतिष्ठित कवि की बात कर रहा हो और उसकी त्रुटियाँ बताकर उसे मेरे ऊपर अपनी सूझ-बूझ का सिक्का ही बैठाना हो ! मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी कविताओं के बारे में भी इस तरह गम्भीरतापूर्वक बात कर सकता है। हम लोग जब भोजनालय से बाहर निकले, तो मैं बहुत कठिनाई से अपनी जम्हाइयों को रोके हुए था और चाह रहा था कि किसी तरह बातचीत का सिलसिला समाप्त हो, तो जाकर सो जाऊँ। रोज़ सुबह चार बजे ही ट्रामों की घरड़-घरड़ और टनन-टनन की वजह से नींद टूट जाती थी जिससे दिन-भर दिमाग़ की नसें तनी रहती थीं। आख़िर फ्लोरा फ़ाउण्टेन तक जाकर मैंने उन लोगों से विदा ली। चलते समय कहा कि मैं दिल्ली आऊँ, तो उससे ज़रूर मिलूँ। मैंने जल्दी ही इसकी हामी भर दी कि कहीं बात और लम्बी न हो जाये। उन्हें छोड़कर लौटते हुए मैं कुछ देर ‘एयर एण्डिया’ के दफ़्तर के बाहर मूँछ और पगड़ीवाले बौने की सूक्तियाँ पढ़ता रहा कि किसी तरह मन की ऊब और झुँझलाहट कुछ कम हो, तो जाकर सोने की कोशिश करूँ। मगर जहाँ तक मुझे याद है, उस रात मुझे तब तक नींद नहीं आयी जब तक नीचे ट्रामों ने सुबह की घण्टियाँ बजाना आरम्भ नहीं कर दिया।
थोड़े दिनों बाद मैं बम्बई छोड़कर दिल्ली चला गया। हरबंस और उसके सारे साहित्य और कला सम्बन्धी बात मैं बम्बई में ही भूल आया था। दिल्ली आकर मैं अपने मित्र अरविन्द के पास ठहरा था जो उन दिनों एक हिन्दी दैनिक में सहायक सम्पादक के रूप में काम कर रहा था। अरविन्द क़स्साबपुरा में अपने प्रेस के एक दफ़्तरी के साथ रहता था। दफ़्तरी, जिसे वहाँ सब लोग ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे, क़स्साबपुरा के उस मुसलमान मुहल्ले में एक टूटे-फूटे घर में नीचे की दो कोठरियों पर कब्जा किये हुए था जिनमें से आगे की कोठरी में अरविन्द रहता था और पीछे की कोठरी में वह स्वयं अपनी पत्नी और सात-आठ साल की लड़की के साथ रहता था। अरविन्द खाना भी उसके यहाँ से ही खाता था और उसे कुल मिलाकर पचहत्तर रुपये महीने देता था। मेरे आने पर पच्चीस, रुपये महीने और देकर उसने मेरे खाने की व्यवस्था भी साथ ही कर दी। दफ़्तरी की पत्नी, जिसे हम कभी ठकुराइन और कभी भाभी कहकर बुलाते थे, बहुत स्नेह और चाव में हमें खिलाती थी। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि वह ठाकुर साहब को उतना अच्छा खाना नहीं देती जितना अच्छा हमें देती है। अरविन्द की जब दिन की ड्यूटी होती थी, तो वह दोपहर का खाना साथ दफ़्तर ले जाता था और जब रात की ड्यूटी होती थी तो ठकुराइन बारह-एक बजे आने पर भी उसे खाना गरम करके ही खिलाती थी। खाना खाते समय अरविन्द ठकुराइन से कुछ-न-कुछ चुहल करता रहता था। ‘ठकुराइन, तर माल तो तुम सब ठाकुर साहब को देती हो; हमारे आगे तो जो रुखा-सूखा बच जाता है वही रख देती हो।’ वह कहता।
‘अभी तुम तर माल के लायक हो कहाँ, लाला ?’ ठकुराइन हँसकर कहती। ‘अभी तो तुम बच्चे हो। तर माल खाओगे, तो बिगड़ नहीं जाओगे ?’’
‘तुम तो ठकुराइन सारी उम्र हमें बच्चा ही बनाये रखोगी,’ अरविन्द कहता। ‘आख़िर हमें किसी तरह बड़े भी तो होना है। हमें कभी तो कुछ खिलाया करो।’
जब खाने लायक हो जाओगे, तो माँगकर नहीं खाओगे,’ ठकुराइन हँसती रहती, ‘पतीली में से निकाल कर खा जाया करोगे। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी, उस दिन ठकुराइन को नहीं पूछोगे। जहाँ पतीली देखोगे, वहीं मुँह मारने लगोगे।’ कहते-कहते ठकुराइन को न जाने क्या लगता कि वह सिर कपड़ा ठीक कर लेती। अपनी मैली धोती के सूराख भी वह जिस किसी तरह ढक लेती।
‘इस तरह कहीं मुँह मारेंगे, तो जूती नहीं खायेंगे ?’ अरविन्द कहता।
‘पकड़े जाओगे तो जूती भी खाओगे। मगर जो जूती से डरता हो, उसे तर माल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, छोटे लाला ?’
मैं हूँ-हाँ में उत्तर देकर कम्बल ओढ़ लेता। ठकुराइन फिर कहती, ‘हमारे छोटे लाला तो बिल्कुल साधु-सन्त आदमी हैं। इन्हें तो रूखा-सूखा भी न मिले, तो भी इनका पेट भरा रहता है। मेरा तो खयाल है इन्हें भूख लगती ही नहीं।’
अरविन्द मेरे चिकुटी काट देता। ‘क्यों बे, बोलता क्यों नहीं ?’
‘ठकुराइन ठीक कहती हैं,’ मैं कम्बल उतारकर कहता।
‘क्या ठीक कहती हैं ?’
‘कि मुझे भूख नहीं लगती। आज सुबह गोभी की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, फिर भी मुझसे सिर्फ़ दो ही रोटी खायी गयीं।’
‘धत्तेरे की !’ अरविन्द मेरे बालों में उँगलियाँ उलझाकर मेरे सिर को अच्छी तरह मल देता ।‘तुझे गोभी के सिवा कुछ सूझता भी है ?’
मैं चुप रहता, क्योंकि मुझे उस समय यह सूझ रहा होता कि कहीं साथ की कोठरी में ठाकुर साहब के खर्राटे सहसा बन्द न हो जायें और मुँह से कुछ कहते-न-कहते मुँह का जायका ही न बदल जाये।
ठकुराइन सिर पर कपड़ा फिर ठीक करती और आँखों-ही-आँखों में मुस्कुराती हुई कहती, ‘ये देखे में जितने सीधे लगते हैं, असल में उतने सीधे हैं नहीं। दुनिया-भर के सब माल खाये हुए हैं। बम्बई रहकर आये हैं। वहाँ तो सुना है कि भाँत-भाँत के पदारथ मिलते हैं।’
अरविन्द एक हाथ से कौर मुँह में डालता और दूसरे हाथ से फिर मुझे थोड़ा गुदगुदा देता और कहता, ‘ठकुराइन, हमारी न सही, कभी तुम इसकी ही कुछ खातिर करो। यह भी क्या कहेगा कि हाँ बम्बई के बाद दिल्ली में भी कुछ दिन रहे थे...’
‘इनसे कहो, ये कहें अपने मुँह से ! बस एक बार कह दें, तो देखो ठकुराइन इनकी ख़ातिरदारी के लिए क्या-क्या नहीं करती ? रोज़ कहें तो रोज़ उन्हें घी की पूरी बनाकर खिलाऊँ।’
‘क्यों बे !’’ अरविन्द अपने जूठे गिलास में हाथ धोकर मुँह पर फेरता हुआ कहता। ‘एक बार कह क्यों नहीं देता ? तेरे बहाने हमें भी घी की पूरी मिल जायेगी। भाभी को तुम ऐसी-वैसी मत समझना, इसका दिल-गुर्दा बहुत बड़ा है।’
‘किससे कह रहे हो लाला ?’ ठकुराइन उसके जूठे बरतन उठाकर चल देती। ‘बेचारे सन्त-महात्मा के पेट में क्यों चूहे दौड़ाते हो ? अभी तो इन्हें तुम नौकरी की ही बात सोचने दो। नौकरी हो जायेगी, तो दुनिया-भर के तर माल भी अपने-आप उड़ाने को मिल जायेंगे। अभी इन्हें तुम रूखे-सूखे पर ही रहने दो।’
ठकुराइन जाकर अपनी कोठरी का किवाड़ बन्द कर लेती, तो अरविन्द कम्बल ओढ़कर लम्बा होता हुआ धीरे से कहता, ‘ठकुराइन है रंगीन-मिज़ाज ! है कि नहीं ?’
‘हाँ है,’ मैं कुढ़े हुए स्वर में कहता। ‘अब मुझे सोने दो।’
‘अच्छा बताओ, तुम क्या सोच रहे हो ? अरविन्द करवट बदलकर मेरे ऊपर को झुका आता।
‘नौकरी की बात सोच रहा हूँ।’
‘धत्त !’ वह मेरी जाँघ को हाथ से मसल देता।‘जैसे नौकरी की बात सोचने का यही वक्त है।’
‘तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकार आदमी हर वक्त एक ही बात सोचता है।’
‘अच्छा यार एक बता बताओ।’ उसका स्वर बहुत धीमा और रहस्यपूर्ण हो जाता।
‘अगर ठकुराइन को थोड़ा और टटोला जाये, तो तुम्हारा क्या ख़याल है इसे पटाया जा सकता है ?’
मैं उसे गुस्से में परे धकेल देता। ‘अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।’
‘मैं तो समझता हूँ कि बस दाना डालने की बात है’, वह सीधा पड़ा-पड़ा कहता। ‘अगर ठीक से दाना डाला जाये तो ऐसी कोई बात नहीं कि ठकुराइन मान न जाये।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book